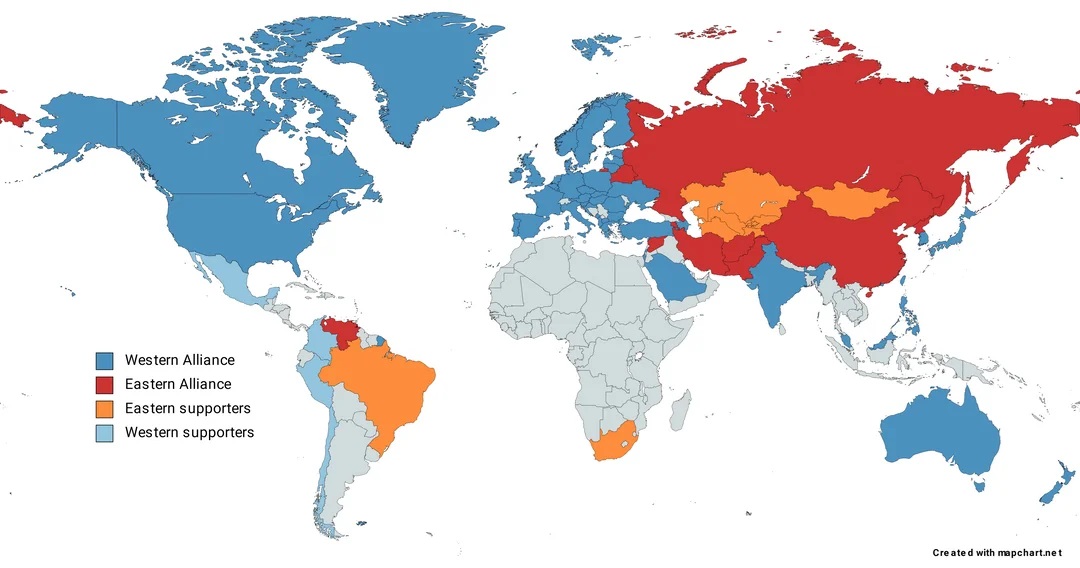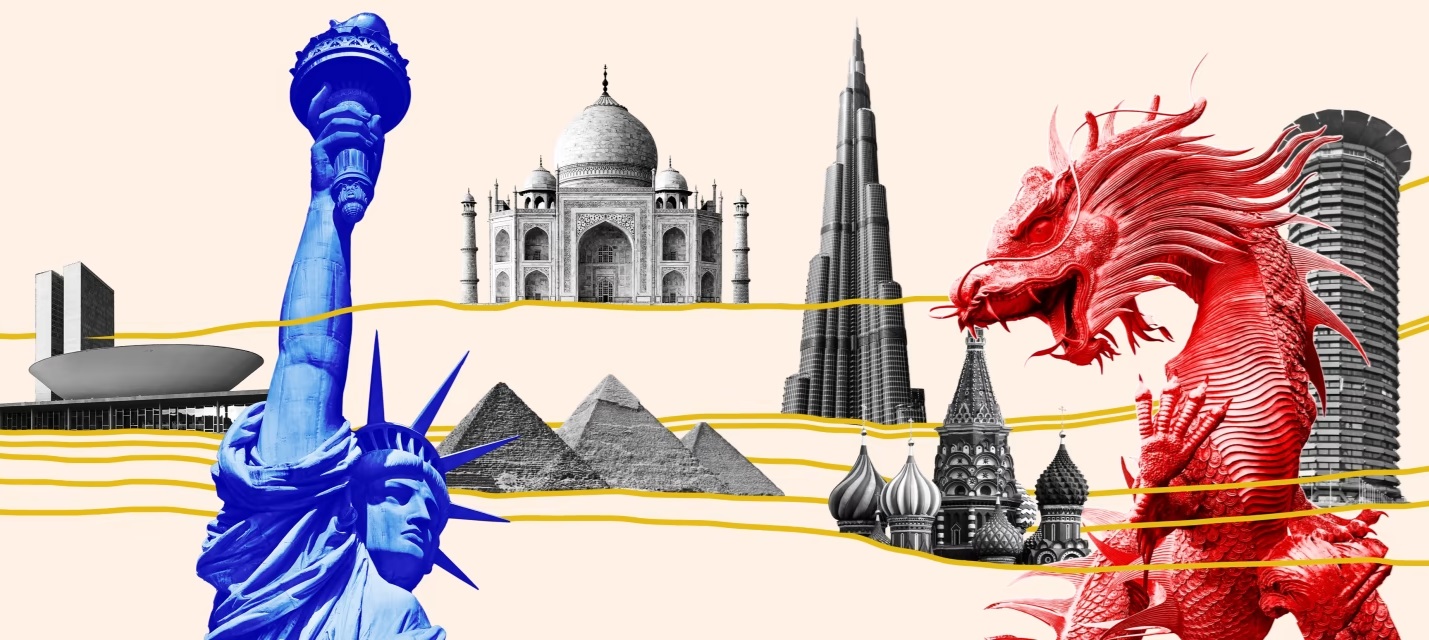History: प्रो हबीब और थापर जैसे इतिहासकारों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं विजय मनोहर तिवारी

(पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी का एक पत्र पढ़ने—लिखने वाली जमात के साथ इतिहास (History) को खबर की सनसनी में मिलाकर चटखारे लेने वालों तक के बीच खासा चर्चित रहा। (इस पत्र का यहां पढ़ा जा सकता है।) उक्त पत्र में श्री तिवारी ने प्रो इरफान हबीब और रोमिला थापर को निशाने पर लेते हुए उन पर मुगल कालीन इतिहास को महिमा मंडित करने और असली इतिहास को छुपाने का आरोप लगाया है। हालांकि इसके पक्ष में वे कोई खास तथ्य उपलब्ध नहीं कराते हैं। पत्र में बीते तीन—चार दशकों से कच्चे दिमागों में भरी गए इतिहास की जानी अनजानी कहानियों की झलक मिलती है और इसे इतनी बार दोहराया गया है कि अब यह कई समूहों को सच प्रतीत होने लगा है। श्री तिवारी भी इन्हीं गल्पों और कुछ फिल्मी कहानियों के जरिये इतिहास के व्हाट्सएप संस्करण पर तुरत फुरत मसले हल करते हुए अपने हीरो और विलेन तय करते हैं। हालांकि इसके बावजूद यह पत्र इतिहास को नए सिरे से पढ़ने, लिखने और स्वीकारने की चुनौती पेश करता है। इतिहास के नवांगुतकों ने कई बेहतर रास्ते खोले हैं और कुछ अनूठे विमर्शों की नींव भी रखी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक खास किस्म की राजनीति और सत्ता के मुफीद आने वाले तर्कों के सहारे लिखा गया यह पत्र भी ऐसे ही किसी विमर्श को खड़ा करेगा। इसी कड़ी में यहां प्रस्तुत है वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के विद्यार्थी सी एन सुब्रह्मण्यम् की यह टिप्पणी। एक निजी समूह में चर्चा के दौरान पोस्ट की गई यह टिप्पणी इतिहास, सनसनी और हमारे समय के सवालों को बहुत खूबसूरती से परखती है। साथ ही उन सवालों के गहरे और सुचिंतित जवाब सामने लाती है, जो इन दिनों एक खास किस्म की राजनीति के तहत उठाकर सोशल मीडिया समूहों के जरिये जन मानस को बरगलाने की साजिश रची जा रही है। संविधान लाइव के पाठकों से अपील है कि इस पत्र को पढ़ते हुए अपने सवाल भी सामने रखें और विमर्श को आगे बढ़ाएं— संविधान लाइव)
श्री विजय मनोहर तिवारी जी की चिट्ठी पर कुछ विचार
सी एन सुब्रह्मण्यम्, होशंगाबाद
मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त, श्री विजय मनोहर तिवारी जी का इरफान हबीब और प्रो रोमिला थापर के नाम पत्र आजकल सामाजिक मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है और हमारे समूह में भी इसकी चर्चा हुई है। किसी ने यह भी पूछा था कि अगर स्व मिश्र जी होते तो उनका क्या जवाब होता। मुझे पता नहीं प्रो. हबीब या प्रो. थापर इसका क्या जवाब देंगे या मिश्र जी की क्या प्रतिक्रिया होती। लेकिन कई मित्रों ने मुझसे पूछा कि मुझे इसके बारे में क्या कहना है। तो मैं तिवारी जी को तो नहीं जानता हूं कि मैं उन्हें यह चिट्ठी भेज दूं, मैं केवल इस समूह के दोस्तों के बीच अपनी बात कहना चाहता हूं।
मैं मानता हूं कि हर नागरिक को और हर इनसान को अपने इतिहास के बारे में और उसे कैसे चित्रित किया जा रहा है इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और संदर्भित इतिहासकारों की पुस्तकों व शोधपत्रों से पढ़कर सीखा हूं। इस नाते मैं अपनी कुछ प्रतिक्रिया रखना चाहता हूं।
तिवारी जी की चिट्ठी के कई पाठकों ने ध्यान दिया होगा कि तिवारी जी कहीं पर भी प्रो. हबीब या थापर की किताबों को पढ़ने का दावा नहीं करते। आगे भी वे कहीं पर भी इन दो इतिहासकारों की किसी खास किताब या शोधपत्र का उल्लेख नहीं करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि तिवारी जी इन दो इतिहासकारों के इतिहास लेखन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, मगर कुछ कल्पित या अनाम इतिहासकारों के काम पर सवाल उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए इस कथन को देखें:
“सल्तनत काल और फिर मुगल काल के शानदार और बहुत विस्तार से दर्ज एक के बाद एक अध्याय। सल्तनत काल के सुल्तानों की बाजार नीतियां, विदेश नीतियां और फिर भारत के निर्माण में मुगल काल के बादशाहों के महान योगदान और सब तरह की कलाओं में उनकी दिलचस्पियां वगैरह।“
अगर किसी ने प्रो थापर की किताबों को सरसरी नजर से भी देखा हो तो उन्हें यह पता होगा कि वे मूलत: प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा करती हैं और एकाध ही उनकी कृतियां होंगी, जिनमें वे 1000 ईसवीं के बाद के काल की चर्चा करती हैं। उनका महत्वपूर्ण काम अशोक और मौर्यों पर था। प्रो हबीब मध्यकाल के इतिहासकार रहे हैं, हालांकि उन्होंने प्राचीन काल और औपनिवेशिक काल पर भी काफी लिखा है। लेकिन जिन लोगों ने प्रो हबीब की किताबों को खासकर उनकी सबसे चर्चित पुस्तक, “दी एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इंडिया“, को पढ़ा होगा, बखूबी जानते होंगे कि इस किताब का उद्देश्य मुगलों का गुणगान करना नहीं, उनका महिमामंडन नहीं, बल्कि ठीक उसके विपरीत यह स्थापित करना था कि किस तरह मुगल साम्राज्य और उसकी सारी शानोशौकत गरीब किसानों के शोषण पर आधारित थी और किस तरह यह शोषण समय के साथ बढ़ता गया और अंत में किसान विद्रोहों में परिणित हुआ जिसके कारण मुगल साम्राज्य अठहारवीं सदी में ढहने लगा। फर्क सिर्फ इतना कि उन्होंने इसे किसी धर्म विशेष के साथ नहीं जोड़ा बल्कि एक खास तरह की सत्ता के ढांचे का परिणाम माना जिसको बनाने में मुगल बादशाह, राजपूत राजा और तमाम लोग शामिल थे।
तिवारी जी की शिकायत है कि इन इतिहासकारों ने जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पर लिखा उन्होंने उसके बाजार में बिक रहे गुलामों के बारे में कुछ नहीं कहा, और वे खासकर गुलाम महिलाओं के बारे में चिंतित हैं। अगर वे इरफान हबीब की एक और बहु चर्चित पुस्तक “दी कैम्ब्रिज एकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया (1200-1750)” पढ़े होते तो पाते कि कम से कम चार पांच पन्नों में सल्तनत कालीन दासता और दास व्यापार के बारे में जितना ब्यौरा इमें स्रोतों से उपलब्ध है, उनका सारांश हबीब पेश करते हैं, सबूतों के साथ।
वैसे इरफान हबीब का मुख्य काम मुगल काल पर रहा है, और सल्तनत काल और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे प्रामाणिक पुस्तक तो प्रो के एस लाल ने लिखी। यह सवाल अगर तिवारी जी प्रो लाल से पूछते तो ज्यादा उचित होता।
वे चलते चलते कहते हैं कि राजघरानों के अरुचिकर इतिहास की जगह गांव गांव में बिखरी बरबाद हो रही सांस्कृतिक विरासत को किसने ध्वस्त किया यह अध्ययन का विषय होता तो इतिहास रुचिकर होता। बतौर उदाहरण वे अपने शहर के मंदिर का उदाहरण देते हैं जिसे सुल्तान इल्तुतमिश ने तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद बनवाया था। उन्हें दुख है कि उस शहर (जिसका नाम वे हमें नहीं बताते) के निवासी और इतिहास शिक्षक इसके बारे में अनभिज्ञ हैं या रुचि नहीं लेते है। उनके उल्लेख से स्पष्ट है कि यह शहर विदिशा ही हो सकता है। बात कुछ इस तरीके से रखी गई है जैसे कि इस अरुचि का कारण इरफान साहब जैसे इतिहासकारों की लीपापोती है। लेकिन यह तथ्य सभी महत्वपूर्ण इतिहास पुस्तकों में पढ़ने को मिलेगा। मैं सिर्फ दो—तीन पुस्तकों का उल्लेख यहां करूंगा— पहला शायद वही किताब है जिसे तिवारी जी ने भी पढ़ा था, वह सैय्यद रिजवी साहब का महान काम जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया था, जिसमें तमाम मध्य कालीन फारसी स्रोतों का अनुवाद हिंदी में किया गया था। (“आदि तुर्क कालीन भारत”, पृ. 28) मध्यकालीन इतिहास के छात्र आमतौर पर प्रो हबीब और खालिक निजामी के दिल्ली सल्तनत नाम की किताब को अपनी टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं और उस किताब में भी इस घटना का विवरण है (पृ. 222)। इसके अलावा रिचर्ड ईटन (जिनके शोध प्रबंधों का अनुवाद डॉ. सुरेश मिश्र ने कभी किया था) ने प्रामाणिक रूप से सुल्तानों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों की सूची में भी इसे शामिल किया है। तो यह समझ नहीं आता कि इस तथ्य को कौन छिपा रहा है ताकि लोगों में सुल्तानों के बारे में खुशनुमा विचार बनें।
विदिशा के मंदिर—मस्जिद (जिसे आज बीजामंडल कहते हैं और जिसका उत्खनन जारी है) शहर के बीच में है और शहर का कोई भी रिक्शावाला आपको वहां तक ले जाएगा और उसके बारे में भी बता पाएगा। तिवारी जी चलते चलते हमें यह आभास भी देते हैं कि इस तरह भारत में कहीं भी कोई ध्वस्त इमारत मिले हम मानकर चलें कि इसे मुस्लिम सुल्तानों ने ही तोड़ा होगा और इतिहास को रोचक बनाना है तो इस खोज में सभी को लग जाना चाहिए कि कौन से सुल्तान ने कब इसे तोड़ा होगा। वैसे हमारे गांव के लोग इतने फिरकापरस्त नहीं हैं और न ही अपनी विरासत के प्रति उदासीन हैं। वे इस बात में दिलचस्पी नहीं लेते कि किसने तोड़ा, मगर इसमें कि इसे हम कैसे सुरक्षित रखें, वे उन अवशेषों को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी मंदिर में या मढिए में स्थापित करते हैं, या फिर जैसे विदिशा के ही मछुआरे समुदाय 2000 साल पुराने होलियोडोरस स्तंभ की खंभ बाबा के नाम से पूजा करते हैं, वैसे आराधना की वस्तु भी बना लेते हैं।
इसके बाद तिवारी जी अपनी मूल बात पर आते हैं— अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और तत्कालीन दास व्यापार। पहले वे बिना किसी आधार के दावा करते हैं कि इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे इतिहासकार अलाउद्दीन की बाजार नीति का महिमामंडन करते हैं। “बरसों तक इतिहास को एक खास पैटर्न पर पढ़ते हुए हमने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीतियों को इस अंदाज से पढ़ा जैसे कि … भारत का शेयर मार्केट आसमान छूने लगा था… जिसने भारत के विकास के सदियों से बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए थे।“
इतिहास में रुचि रखने वाले पाठकों से मेरा आग्रह होगा कि वे इरफान हबीब के “दी कैम्ब्रिज एकानामिक हिस्ट्री आफ इंडिया” के प्रथम वाल्यूम में इस विषय पर लिखे अध्याय (पृ. 86—89) को पढ़ें और बताएं कि क्या दूर दूर तक तिवारी जी का कथन सही है? हबीब इस नीति की विवेचना करते हैं और हमें बताते हैं कि यह केवल दिल्ली के आसपास के इलाकों पर लागू हुई होगी और इसका मकसद सैनिकों व कामगारों के वेतन को कम रखना था और वास्तव में गरीब वैतनिकों व मजदूरों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ और वे हमें यह भी बताते हैं कि अलाउद्दीन के मरते ही यह व्यवस्था टिक नहीं पाई। इरफान हबीब ने यहां पूर्व के इतिहासकार बनारसी प्रसाद सक्सेना के निष्कर्षों को चुनौती दी — सक्सेना जी कुछ सीमित हद तक इन नीतियों का गुणगान करते दिखते हैं वे उन बाजारों में बिक रहे गुलामों के बारे में चिंतित नहीं हैं। शायद यह महज इत्तेफाक नहीं है कि इरफान हबीब की पुस्तक में अलाउद्दीन की बाजार नीति की चर्चा के बाद तुरंत अगला उपशीर्षक का विषय गुलामी ही है और उन बाजारों में बिक रहे गुलामों के बारे में है। (देखिए पृ 89—93)
लेकिन तिवारी जी का आग्रह है कि हम शासकों व उनकी नीतियों का महिमामंडन करने से पहले या कम से कम साथ साथ उन बातों पर भी नजर डालें जो अप्रिय हैं, जैसे कि लोगों को युद्ध में गुलाम बनाना और उपासना स्थलों की पवित्रता को भंग करना। इनका अपने देश में बहुत लंबा इतिहास है जो शायद अभी तक ठीक से लिखा नहीं गया है। मैं यहां दास प्रथा और खासकर युद्ध में हारे हुए लोगों (पुरुष व महिलाओं) को गुलाम बनाकर ले जाने की प्रथा के इतिहास की चर्चा करूंगा।
तिवारी जी बात को कुछ इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे कि युद्ध में महिलाओं व पुरुषों को बंदी बनाकर लाना, उन्हें बेचना या उपहार दान में देना, वगैरह पहली बार सल्तनत काल में हो रहा था। उससे वे बहुत सारे निष्कर्ष निकालते हैं, जिनकी चर्चा कुछ बाद में करूंगा। यहां मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि युद्ध में गुलाम बनाना विश्व भर में एक प्राचीनतम परंपरा थी जिसपर लगभग उन्नीसवीं सदी में जाकर रोक लगी और युद्ध बंदियों से मानवता के साथ व्यवहार करने की परिपाटी शुरू हुई।
भारत में वैदिक काल को ही लें जब से हमें साहित्यिक साक्ष्य मिलने लगते है। हम सब जानते हैं कि दास और दासी शब्द ही वैदिक काल की देन हैं, जब दासा और दस्यु नामक विरोधी लोगों को युद्ध में हराकर बंदी बनाया जाने लगा था और गुलाम और — एक जातीय समूह — दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग हुआ। सबसे प्राचीन वेद, ऋगवेद में दानस्तुतियां हैं, जिनमें अनेकों दासियों को राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिए जाने का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण (यह भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है) में एक राजा द्वारा अपने पुरोहित को 10,000 दासियां दक्षिणा में देने का उल्लेख है। इस संख्या को अतिश्योक्ति मानें तो भी यह तो नकारा नहीं जा सकता है कि उन दिनों दासियों को पुरोहितों को दान में देने की प्रथा थी। दान में पुरुष दासों का उल्लेख अपेक्षया कम है जबकि दासियों का उल्लेख अधिक है। धर्मशास्त्रों में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को गुलामी का एक वैध स्रोत माना गया है। अशोक ने कबूल किया था कि कलिंग विजय के बाद वहां से डेढ़ लाख लोग गुलाम बनाकर ले जाए गए। हो सकता है कि संख्या में कुछ अतिश्योक्ति हो, मगर मुद्दे की बात यह है कि युद्ध में लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उन्हें अपने वतन से दूर ले जाया जाता था। यह प्रथा कभी खतम नहीं हुई और हम पूर्व मध्यकाल में भी इसको फलते फूलते देखते हैं।
भारतीय इतिहास में चोल वंश और चालुक्य वंश का बड़ा नाम है। समकालीन चीनी यात्री हमें बताते हैं कि चोल राजा के अंत:पुर में दस हजार नाचने वाली लड़कियां थीं जो संभवत: दासियां थीं। यह अतिश्योक्ति लगता है मगर चालुक्य कालीन निर्माण कला ग्रंथ मानसार में कहा गया है कि राजा के महल में लाखों महिलाओं के लिए प्रबंध होना चाहिए। चोल राजाओं की प्रशस्ति में अंकित है कि वे किस तरह विरोधी राजाओं की महिलाओं को अपने महल में दासी बनाकर रखते थे। तमिल साहित्य में दर्ज है कि राजधानी में अलग अलग महलों में विभिन्न देशों में बंदी बनाकर लाई गई महिलाएं होती थीं जिन्हें राजा के जुलूस का स्वागत करना होता था। युद्ध में विरोधी खेमे की महिलाओं को दासी बनाने के अलावा गांव शहर की महिलाओं को बंदी बनाकर लाना या फिर वहीं उनके साथ बलात्कार करना सामान्य बात थी। कर्णाटका के धारवाड जिले से सन 1007 का एक शिलालेख है जिसमें चोल सैनिक अभियान का विवरण दर्ज है, कि किस तरह पूरा राज्य लूटा गया, महिला, बच्चे और ब्राह्मणों को मारा गया और महिलाओं को बंदी बनाया गया और वर्ण व्यवस्था को भंग किया गया। वर्ण व्यवस्था भंग करना व्यापक बलात्कार की ओर इशारा करने वाला रूपक था। हमें ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि राजा अपने महल की दासियों को मंदिरों को दान में दे देते थे। शिलालेख बताते हैं कि तब उन महिलाओं पर राजा की निशानी को मिटाकर मंदिर की निशानी अंकित की जाती थी (जैसे कि गाय बकरियों के साथ किया जाता था)।
उत्तर भारत से इस तरह की जानकारी अपेक्षाकृत कम है, मगर लेखपद्धति में दर्ज मॉडल दस्तावेजों में एक है “दासी विक्रय पत्र“। इसमें बताया गया है कि किसी राणा प्रताप सिंह ने दूसरे राज्य पर चढ़ाई की और वहां से पनूती नामक सोलह साल की लड़की को उठाकर लाया और उसे नगर के प्रमुखों को सूचित करने के बाद नगर के चौरास्ते पर नीलाम कर दिया और उस लड़की को एक व्यापारी ने अपने घरेलू काम के लिए खरीदा। दस्तावेज में उसके कामों का वर्णन है जिसमें टट्टी साफ करने से लेकर साफ सफाई, दूध दुहना, खेतों का काम आदि की सूची है। दस्तावेज में यह भी दर्ज है कि अगर यह लड़की हताश होकर आत्महत्या करती है तो वह गधी या चांड़ाली का जन्म लेगी और उसके मालिक पर कोई पाप नहीं लगेगा। यह ऐसे दासी विक्रिय पत्रों का प्रारूप है, यानी यह केवल इकलौती घटना नहीं है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में दास दासियों के वर्णनों की भरमार है जिन्हें दोहराने की जरूरत यहां नहीं है।
यहां दो बातें कहना जरूरी है। पहली बात यह है कि दासता का कोई एक रूप नहीं था मगर उसमें बहुत विविधता थी, कुलीन दास—दासियों से अलग व्यवहार होता था और हमें कई दास दासियों का उल्लेख मिलता है जिनके पास धन दौलत भी थी। दूसरी ओर पनूती जैसे लोग भी थे। कुछ इसी तरह की विविधता सल्तनत काल में भी मिलती है जहां कोई सुशिक्षित और चतुर दास सुल्तान बनने या कम से कम उंचे ओहदे पर पहुंचने की आशा कर सकता था और दूसरी छोर पर अत्यंत दयनीय हालातों में काम करने वाले दास दासियां भी थे। मध्यकालीन दासता काफी जटिल और विविध संस्था थी। दूसरी बात यह है कि दास प्रथा और दास व्यापार सल्तनत के दौरान तेजी से बढ़ी और सुल्तान फिरोज शाह के समय तक आते अपनी चरम पर पहुंची। लेकिन उसके बाद इसमें तेजी से कमी आई और मुगल काल में यह काफी सीमित स्तर पर रही। इस जटिल इतिहास को हम सरल तरीकों से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हाल में इस विषय पर कई विद्वानों ने बारीक अध्ययन किया है और कुछ नाम मैं नीचे संलग्न पुस्तक सूची में दूंगा।
वैसे तिवारी जी की दिलचस्पी मध्यकालीन दास प्रथा में उतनी नहीं है जितना यह जताने में है कि वर्तमान समय के अधिकांश मुसलमान वास्तव में उन बालात गुलाम बनाकर मुसलमानों को दी गई दासियों के वंशज हैं। वे इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमानों की मूल पहचान यही है कि वे सब बलात गुलाम बनाई गईं हिंदू दासियों और आक्रांता बापों की औलाद हैं। इस तरह वे बलात धर्मांतरण सिद्धांत का एक नया रूप पेश करते हैं।
पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तिवारी जी का दावा है, जिसके समर्थन में केवल यह तथ्य पेश किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में बड़ी तादात में महिलाएं गुलाम बनाकर लाई गईं। कुल कितने गुलाम दिल्ली के बाजारों में बिके होंगे और उनमें से कितनी महिलाएं थीं, क्या यह तादात उतनी थी कि दक्षिण एशिया के आज के करोड़ों मुसलमानों की वे ही पूर्वज रही होंगी, ऐसे सवालों में तिवारी जी प्रवेश नहीं करते हैं। एक और सवाल जो काफी पहले रिचर्ड ईटन ने उठाया था कि ऐसा क्यों है कि दक्षिण एशिया से सर्वाधित मुसलमान सल्तनत या मुगल सत्ता के केंद्रीय प्रदेशों में नहीं पाए जाते, और सुदूर, केरल (जहां उनकी सत्ता नहीं थी), बंगाल, कश्मीर और पंजाब जैसे प्रांतों में बसे हैं? क्या ऐसा कुछ हुआ कि उन गुलाम महिलाओं को लेकर वे मुसलमान इन दूर दराज के इलाकों में बसने चले गए थे? यह भी फिट नहीं बैठता क्योंकि उदाहरण के लिए बंगाल का इस्लामीकरण वास्तव में मुगल शासन के खात्मे के दौर यानी 18वीं सदी में हुआ। दक्षिण एशिया में इस्लाम के फैलने में जरूर सल्तनत और मुगल सत्ता से मदद मिली होगी, मगर करोड़ों लोगों का किसी धार्मिक संस्कृति में शामिल होना इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है और इसे समझने के लिए हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में हो रहे बदलावों को समझना होगा। रिचर्ड ईटन बंगाल के संदर्भ में गहन अध्ययन के बाद एक मॉडल पेश करते हैं, जिसे पढ़ें तो उस पर विमर्श और बहस की जा सकती है।
लेकिन तिवारी जी ने मुझे एक और प्रसंग की याद दिलाई जो यहां पर मौजूं भी है। वर्तमान में लोगों के डीएनए की बड़ी चर्चा होती है। इंडो यूरोपियन भाषी समूहों के डीएनए परीक्षण से पता चलता है कि इस भाषा को बोलने वाले लोग जो यूरेशिया में ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में फैले, वे मुख्य रूप से पुरुष ही थे जिन्होंने जहां भी वे पहुंचे वहां की स्थानीय महिलाओं से संबंध बनाकर बच्चे पैदा किए। जो लोग इस पर और जानना चाहते हैं वे टोनी जोसेफ की पठनीय पुस्तक को जरूर पढ़ें। यही पैटर्न भारत सहित अधिकांश देशों में देखने को मिलता है।
अगला मुद्दा जो तथ्यों से संबंधित है वह है यह दावा कि भारत की संस्कृति चारों तरफ एक जैसी ही फलती फूलती रही। भले ही इस देश में राजनैतिक एकता न रही हो। वे यह दावा करते हैं कि इरफान हबीब और थापर जैसे इतिहासकार इस बात को जानबूझकर नजरंदाज करते हैं और यह आभास देते हैं कि मुगलों ने ही भारत राष्ट्र का निर्माण किया। पहले की तरह मैं यह कहना चाहता हूं कि न इरफान हबीब ने न रोमिला थापर ने कभी दावा किया कि इस उप महाद्वीप जिसे हम भारत कहते हैं, की मुगल काल से पहले कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं थी। अगर आप रोमिला थापर की चर्चित पुस्तक अर्ली इंडिया पढ़ेंगे तो शायद आप देख पाएंगे कि वे यही चर्चा करती हैं कि यह सांस्कृतिक पहचान बनी किस तरह और उसमें निहित तत्व क्या क्या थे और उनका आपसी संबंध क्या था और वे बदले या विकसित कैसे हुए। अगर उनके लेखन में कहीं भी यह आभास हुआ हो कि 1550 से पहले भारत की सांस्कृतिक पहचान नहीं थी तो कोई पाठक मुझे बताएं। रहा सवाल इरफान हबीब का। मैं पाठकों से आग्रह करूंगा कि वे उनका 1997 में प्रकाशित लेख दी फारमेशन आफ इंडिया को पढ़ें। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मौर्य काल से ही इस उपमहाद्वीप की दूसरे देशों अलग सांस्कृतिक पहचान बनने लगी थी। कुल मिलाकर तिवारी जी इन इतिहासकारों पर एक कल्पित आरोप लगा रहे हैं और फिर उन्हें भारतीय विरोधी कहकर उनके तमाम काम को नकारना चाहते हैं। तिवारी जी का नजरिया और इन इतिहासकारों के बीच अगर फर्क है तो वह एक ऐतिहासिक नजरिए का है। ऐतिहासिक नजरिया मानता है कि कोई भी चीज कभी, किसी प्रक्रिया से बनती है। वह अनादिकाल से मौजूद नहीं होती है। अगर हम यह मानें कि भारत एक सांस्कृतिक इकाई है तो यह किसी समय नहीं रही होगी और किन्हीं प्रक्रियाओं के जरिए, किन्हीं लोगों के प्रयास से समय के साथ बनी होगी या लंबे समय के अंतराल में विकसित हुई होगी। इतिहासकार का काम है कि इस प्रक्रिया को समझना और उजागर करना। इतिहासकार यह कहकर नहीं बच सकता कि हजारों सालों से या उससे भी पहले से ऐसा ही था। तो इरफान हबीब हों या रोमिला थापर इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि यह कब और कैसे बना, किस हद तक बना, उसके अवयव क्या हैं और आज उसकी क्या स्थिति है वगैरह। मिसाल के तौर पर तिवारी जी का दावा है कि सोमनाथ से केदारनाथ तक ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की परंपरा हजारों साल पुरानी है। अब इस कथन में निहित भावना है कि यह अनादिकाल से चला आ रहा है। अगर मैं यह सवाल करूं कि हमारे पास सोमनाथ और केदारनाथ में मंदिर, शिवमंदिर सहित मंदिरों के अवशेष या उल्लेख कब से मिलते हैं, उस इलाके में मानव बसाहट कब से शुरू हुई, वगैरह तो यह कहना उतना आसान नहीं होगा कि यह हजारों साल पुरानी परंपरा है। उन साहित्यिक स्रोतों में जिनमें सबसे पहले हमें ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, उनका भी काल निर्धारण भारतीय साहित्य के प्रकाण्ड विद्वानों ने किया है। इन सबको शैवधर्म के इतिहास के संदर्भ में देखने पर हम कुछ निर्णय पर पहुंच सकते हैं। भारतवर्ष की अवधारणा के विकास पर इतिहासकार ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण काम है और मैं पाठकों से आग्रह करूंगा कि उनके लेख को जरूर पढ़ें।
इतिहासकार स्रोतों को सनसनीखेज खबरों को ढूंढने या सूचनाओं को उनके संदर्भ से दूर करके प्रसारित करने के लिए पढ़ते हैं, वे स्रोतों को परखते हैं, उनमें मिली खबरों व सूचनाओं को भी परखते हैं, उन्हें अपने ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर उनके कार्यकारण संबंध खोजते हैं। शायद इसलिए उनका काम ऐसा रोचक नहीं लगता कि उसे व्हाट्सएैप मैसेज के रूप में प्रसारित किया जा सके।
अंत में एक बात रखना चाहता हूं तिवारी जी के तथ्यों के बारे में नहीं बल्कि उनके नजरिए के बारे में। जाने अनजाने वे इतनी खूबसूरत भाषा का उपयोग करते हैं जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को दर्शाता है। उनकी अपेक्षा मेरी भाषा ज्यादा संकीर्ण है। भाषाएं सिर्फ शब्द और उनके अर्थ नहीं होते हैं और वे अपने साथ एक तजुर्बा और तहजीब लेकर आते हैं। तिवारी जी की भाषा में जो तहजीब है वह दर्शाता है कि हमने अपने हजारों वर्षों के इतिहास को खासकर पिछले पांच सौ वर्षों के इतिहास को आत्मसात किया है। भले ही उन्हें यह इतिहास आतंक से भरा लगता है। कुछ हद तक वे सही भी हैं कि इन शताब्दियों में हमारे शासकों ने प्रेम और सहृदयता का कम ही परिचय दिया और जुल्म और हिंसा की कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर यह केवल इन पांच सौ सालों की बात नहीं है। इतिहास का हर पन्ना चाहे वह हजारों साल पुराना हो या आज का, एक तरफ रक्त रंजित है और दूसरी ओर सृजन, मानवीयता और ज्ञान के विस्तार भी उन्हीं खून के निशानों के बीच अंकित हैं। जब अशोक, समुद्रगुप्त, राजेंद्र चोल, बुक्क की सेनाएं चलीं तो उनका सामना करने वालों ने खुशियां तो नहीं मनाई होंगी। उन्होंने जो शासन व्यवस्थाएं बनाईं वो सबके पसंद की भी नहीं रही होंगी। लेकिन इन राजाओं ने खूबसूरत और भव्य इमारतें बनवाईं, साहित्य, धर्म और कलाओं के महान मनीषियों को आश्रय भी दिया जो आज हम अपनी विरासत में गिनते हैं। लोगों के बीच विचारों, ईश्वर की कल्पना व सौंदर्यबोध का लेन देन भी चलता रहा और खून खराबे के बीच लोगों की संस्कृति निरंतर समृद्ध होती गई। मैं इसका एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ जिसमें कोई जीता कोई हारा और हजारों मारे गए। मगर आज वहां के लोग उसी खून से रंगी मिट्टी में गुलाब की खेती करते हैं और इत्र और गुलकंद बनाकर सुगंध और मिठास फैलाते हैं। कहते हैं कि गुलाब के पौधे मुगल सैनिकों ने लगाए थे। राजा और बादशाहों की बातें छोड़ भी दें तो हम और आप भले ही दूध से धुले न हों, मगर हम सब भी तो उस सांझी सुंदरता, मानवता और विरासत को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे न हो कि हम केवल एक पक्ष को देखें और दूसरे की सीख को खो दें।
कुछ संदर्भ ग्रंथ
1. Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal India, OUP, New Delhi
2. Tapan Raychaudhuri & Irfan Habib, The Cambridge Economic History of India, I, 1200-1750
3. Irfan Habib, ‘The Formation of India- Notes on the History of an Idea’, Social Scientist, Vol.25, No. 7/8 (Jul. – Aug., 1997), pp. 3-10
4. Romila Thapar, The Penguin History of Early India, From Earliest Times to AD 1300, 2002
5. B D Chattopadhyaya, The Concept of Bharatavarsha and other Essays, SUNY Press, 2018
6. KS Lal, History of the Khaljis, Allahabad 1950
7. Mohd Habib & KA Nizami, Comprehensive History of India Vol V, Delhi Sultanate, PPH, New Delhi 1982
8. PV Kane, The History of Dharmasastras, Vol 2
9. RC Hazra, Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs, Motilal Banarasidas, Delhi 1987
10. Richard M Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, OUP, 1993
11. Richard M Eaton, Temple Desecration and the Muslim Sultanates of medieval India, 2004