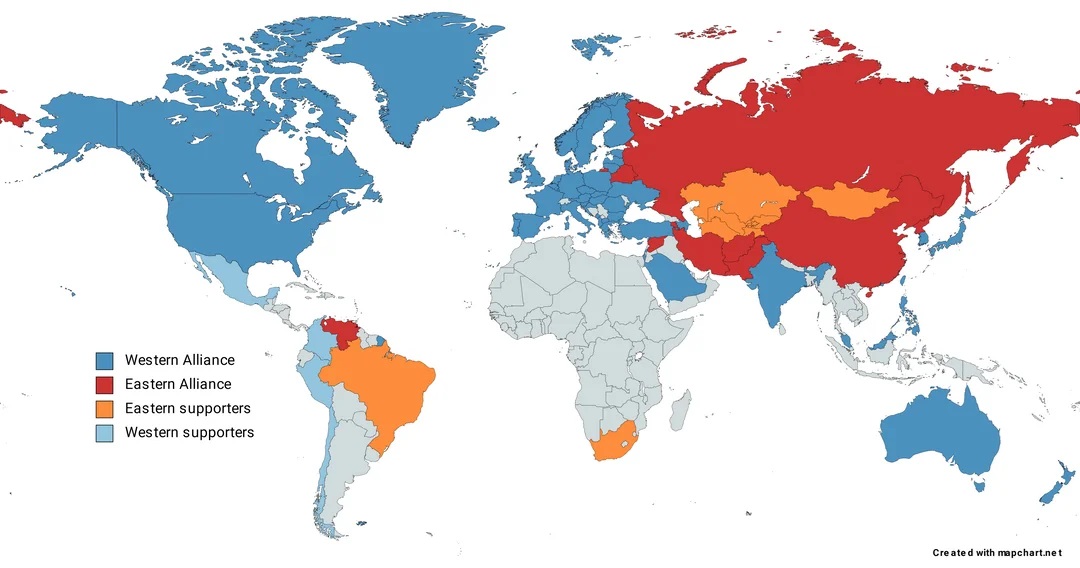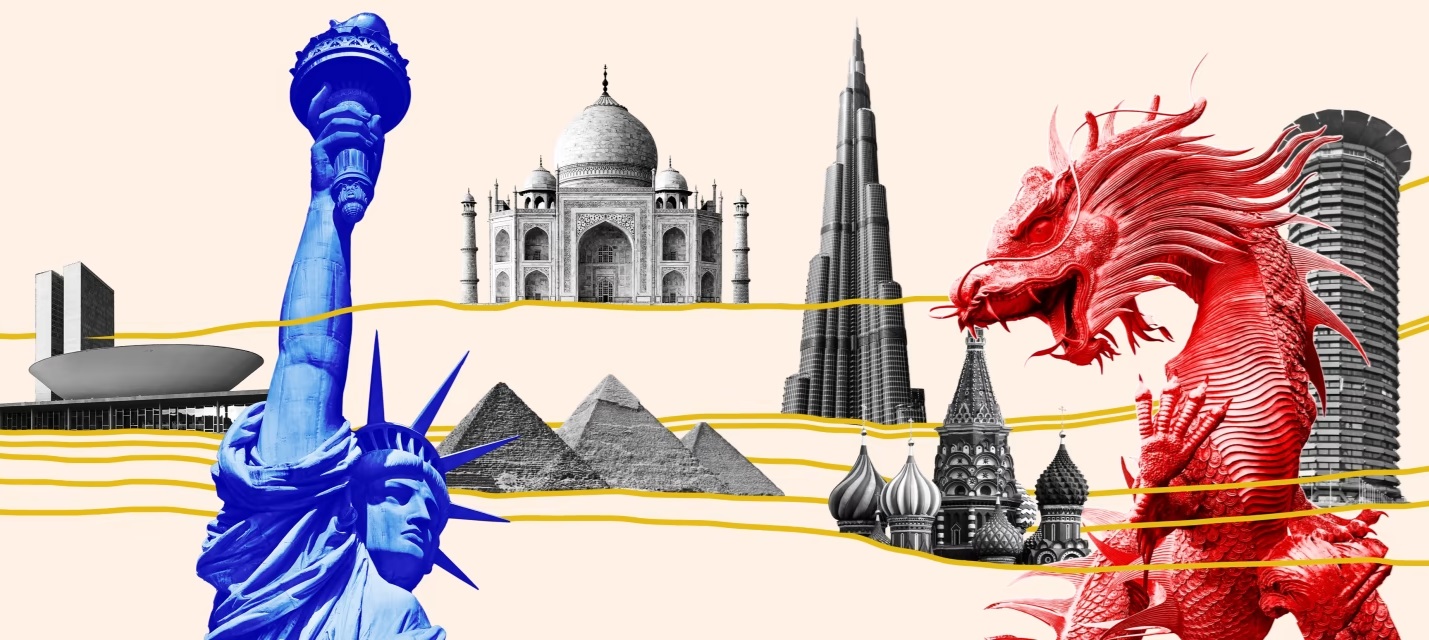Farmers Movement: खेती को मुख्यधारा में लाता आंदोलन
 (दिल्ली की चौहद्दी पर पिछले करीब एक महीने से जारी किसान आंदोलन (Farmers Movement) ने खेती-किसानी को कम-से-कम बहस के लायक तो बना ही दिया है। इस लिहाज से देखें तो पिछले तीन-साढ़े तीन सप्ताह देशभर के लिए कृषि-प्रशिक्षण का बेहतरीन मौका देने वाले रहे हैं। प्रस्तुत है, इसी विषय पर टिप्पणी करता वरिष्ठ पत्रकार डॉ. संतोष पाटीदार का यह लेख।)
(दिल्ली की चौहद्दी पर पिछले करीब एक महीने से जारी किसान आंदोलन (Farmers Movement) ने खेती-किसानी को कम-से-कम बहस के लायक तो बना ही दिया है। इस लिहाज से देखें तो पिछले तीन-साढ़े तीन सप्ताह देशभर के लिए कृषि-प्रशिक्षण का बेहतरीन मौका देने वाले रहे हैं। प्रस्तुत है, इसी विषय पर टिप्पणी करता वरिष्ठ पत्रकार डॉ. संतोष पाटीदार का यह लेख।)
इस साल जब कोरोना लॉकडॉउन खुला तो खेती-किसानी के नए कानून, ‘लुटियंस’ दिल्ली में खड़ी संसद में लॉक होने जा रहे थे। बाद में सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कानूनों को आखिर विरोध का सामना करना ही पड़ा। इसका अंदाजा सरकार को नहीं था और कानून के विरोध को हंसी-खेल मान लिया गया था। नतीजे में नए कृषि कानूनों की मुखालिफत हर दिन बढ़ती गई। मात्र तीन हफ्तों में खेती के कानूनों का हल्ला गाँवों की चौपाल तक पहुंच गया। सरकार के साथ सत्ताधारी संगठन भाजपा ने अभियान चलाते हुए कानून के फायदे गाँव-गाँव में चौपाल लगाकर बताने की मुहिम छेड़ी है। किसी भी सरकार द्वारा विरोध का जवाब देने का इससे बेहतर प्रयास क्या होगा? लेकिन सरकार को यह काम कानून बनाने के पहले करना था। अब मजबूरी वश करना पड़ रहा है तो भी इससे खेती-किसानी का ही फायदा है। दोनों ओर से सोते—जागते, उठते-बैठते सारा जोर खेती पर है। राष्ट्र के केंद्र में इस तरह खेती शायद पहली बार आई है।
आंदोलन द्वारा सरकार के विरोध और सरकार समेत सत्ताधारी पार्टी द्वारा आंदोलन के खिलाफ मोर्चा लेने से खेती के प्रति देशभर में बड़ा जनजागरण हो गया है। दोनों मामलों में खेती किसानी की बेहतरी ही है। यह भी कह सकते हैं कि किसान आंदोलन ने सरकार के साथ राजनीतिक दलों व नौकरशाहों सहित सबको खेती के महत्वपूर्ण काम से लगाने का ऐतिहासिक काम कर दिया है। कानूनों और आंदोलन का जो भी हो, पर फिलहाल यह किसानों की बड़ी जीत है। तमाम मुसीबतों से जूझते आंदोलन की अहिंसात्मक एकजुटता की मजबूत ताकत ने देश को खेती की महत्ता व गांवों की असीम शक्ति का एहसास करा दिया है। किसानों के आगे इस कथित मजबूत सरकार की लाचार स्थिति देख गाँव, खेत व किसान से दूर होती युवा पीढ़ी और देश की जनता को खेती-बाड़ी की अनिवार्यता अच्छी तरह समझ आ गई है।
अंग्रेजों द्वारा खेती को जान-बूझकर उपेक्षित किया गया था। आजादी के बाद भी खेती-किसानी का गला घोंटने की नीतियां बनाना ही सरकारी शगल बना हुआ था। आजाद भारत में “जी-हुजूरी” में रत नौकरशाही के एक बड़े तबके पर अंग्रेजों की मानसिकता हावी है। किसानों के हित में किसानों से सलाह-मशविरा किए बिना आधे-अधूरे कानून बनाना किसानों के प्रति सरकार की गम्भीरता में कमी दर्शाता है।
फसलों के ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) की तरह ही इस समय राजनीतिक दलों (सत्ताधारी और विरोधी पक्ष) के लिए खेती ”न्यूनतम राजनैतिक वोट” हासिल करने का सबब बन गई है। ‘इंडिया’ की सरकार, समाज और मीडिया सहित देश की नजरों में ‘भारत’ राष्ट्र के गाँव, खेत, खलिहान व किसान कल तक दोयम दर्जे के रहे थे, पर आज किसानों के सड़क पर आते ही दृश्य बदल गया है।
इस मायने में, सरकार के साथ बन्दर-गुलाटी खाते मीडिया में “हिकारत भरी नजरों” से देखी जाने वाली खेती को किसान आंदोलन ने प्राइम टाइम का “हाई प्रोफाइल” ईश्यू बना दिया है। मीडिया को अच्छे से समझ आ गया है कि खेती-किसानी दोयम नहीं, वरन देश की आवाज के साथ टीआरपी व करोड़ों के सरकारी विज्ञापनों की फसल बटोरने वाली बड़े उपभोक्ता बाज़ार की ‘दूध देती गाय’ है।
जो भो हो, ‘गोदी मीडिया’ के बड़े तबके के माध्यम से किसानों के विरोध को टुकड़े-टुकड़े करने की जंग हर संभव तरीकों से लड़ी जा रही है। इस जंग में ‘टुकड़े- टुकड़े गैंग’ जैसे निरर्थक जुमले भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। यह बताता है कि चुनौती देते किसानों के तीखे तेवर सरकार की परेशानियां बढ़ा रहे हैं।
खेती के नए कानून के खिलाफ खड़े किसानों की मुखालिफत में केंद्र सरकार व भाजपा के सलाहकार परम्परागत कोशिशों से प्रायोजित प्रपोगंडा के साथ मैदान लड़ा रहे हैं। दूसरी ओर, अपने हितों व व्यवसायिक स्वार्थों की ख़ातिर उत्तर-भारत के छोटे, बड़े, मझौले किसान, मजदूर, आढ़तिये, व्यापारी सभी किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। वामपंथ, मध्यपंथ आदि के खुले समर्थन और दक्षिण पंथीय एक बड़े किसानी वर्ग का मौन समर्थन भी आंदोलन की प्रमुख मांगों के साथ है। किसानों के साथ लाल, हरा, केशरिया, सफेद (गाँधीवादी) सभी रंग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घुले-मिले हैं। सरकार के संकटमोचक इस पर चाहे ‘लाल’ या ‘हरा’ रंग पोतें, राष्ट्रवादी किसान बेफिक्र नजर आते हैं।
सरकार विरोध की कहानी कहता यह आंदोलन इतिहास दोहराने की कोशिश भी कर रहा है। करीब 30 बरस पहले 1989 में उत्तरप्रदेश में किसान यूनियन के नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के साथ केंद्र सरकार के विरोध की जंग मेरठ कमिश्नरी के घेराव से शुरू की थी जो अंत में दिल्ली में खत्म हुई थी। उस समय की राजीव गांधी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा था। स्वर्गीय टिकैत को उस आंदोलन ने देश में किसान नायक बना दिया था। अब उनके पुत्र राकेश सिंह टिकैत इस आंदोलन के प्रमुख किरदारों में से एक हैं। कानून वापसी की मांग पर अड़िग आंदोलन की कमर तोडने के सारे उपाय कर रही सरकार भी सिर्फ कानून संशोधन पर अडी है। सरकार की अपनी मजबूरी है, वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती। दूसरी ओर, किसानों को सरकारी तंत्र की हकीकत से रोज जूझना होता है, इसलिए वे सरकारी दावों पर भरोसा नहीं कर सकते।
इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकार वाकई में खेती की खातिर आमूलचूल बदलाव चाहती है। माना जा सकता है कि नए कानूनों की रचना इसी मकसद से हुई हो। फिर कमी कहां रह गई?लगता है हर समस्या का हल पूंजीवाद पर टिके निजीकरण को मानने वाले अर्थशास्त्रियों व नौकरशाही ने जमीनी सच्चाई से आंख मूंदकर कानून बनवा दिये। इन लोगों ने नए विचार व ठोस उपाय ढूंढ़ने की तकलीफ नहीं उठाई। इसके बजाए पुरानी सरकारों के जमाने में खेती की बेहतरी के लिए बनी आधी-अधूरी सिफारिशी रिपोर्ट्स व देशी-विदेशी कार्पोरेट घरानों के हाथ खेत-खलिहान की सुरक्षा की कल्पना को आधार बना लिया। सरकार ने, हो सकता है, गुजरात जैसे एक राज्य में आजमाए खेती-किसानी के पुराने मॉडल को पूरे देश के लिए उपयुक्त मान लिया हो। जबकि भौगोलिक रूप से विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फैले देश के लिए एक राज्य के प्रयोग कारगर नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसानों से सलाह-मशविरा किए बिना कानून बनाने के परिणाम से अफसर व सत्ताधारी नेता बेखबर रहे। यही कारण है कि अब सरकार उहापोह की स्थिति के साथ कठघरे में है।
ऐसा इसलिए भी कि आरएसएस के प्रमुख किसान संघ के बड़े पदाधिकारी के हवाले से प्रकाशित समाचार में कहा गया है कि कानून बनाने के समय हमने सुझाव रखने की कई कोशिशें कीं, पर अफसर मिलने का समय तक नहीं देते थे। यही नहीं, जो सुझाव भेजे गए उन पर भी बात नहीं की, न ही कोई जवाब दिये। जाहिर है, कहीं-न-कहीं बड़ी गड़बड़ हुई। नए कानून आते ही किसान संघ ने शीर्ष स्तर पर अन्य कमियों के साथ आपत्ति जताते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की मांग की थी। यह आवाज कहीं दबा दी गई। कहा जा रहा है, खेती के अनुभवी किसानों व संगठनों को कानून बनाने की प्रक्रिया से दूर रखने से संकट खड़ा हो गया है। क्या देश से ‘मन की बात’ करते प्रधानमंत्री के नौकरशाहों ने किसानों के मन की बात सुनने के साथ रायशुमारी जैसी कोई जरूरत नहीं समझी, न ही इसके लिए उन्हें कहा गया?
जैसा मध्यप्रदेश के पूर्व किसान संघ नेता व अब ‘राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन’ के प्रमुख शिवकुमार शर्मा ‘कक्काजी’ ने एक टीवी चैनल की परिचर्चा में बताया था कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ बीते दिनों आंदोलन के 13 नेताओं की मीटिंग हुई थी। बैठक में श्री शाह ने स्वीकारा कि कानून बनाते समय किसान नेताओं से चर्चा नहीं होने की गलती हुई, पर अब तो चर्चा हो सकती है। यह इससे भी स्पष्ट है कि उदारमना किसानों के प्रति संजीदा सरकार ने ईमानदारी से आंदोलन की प्रमुख मांगों के मद्देनजर कानून में कमी स्वीकारी। यह अच्छी शरुआत है। बशर्ते, ऐसे भाव सरकार के अंतर्मन से भी हों!
(सर्वोदय प्रेस सर्विस से साभार)