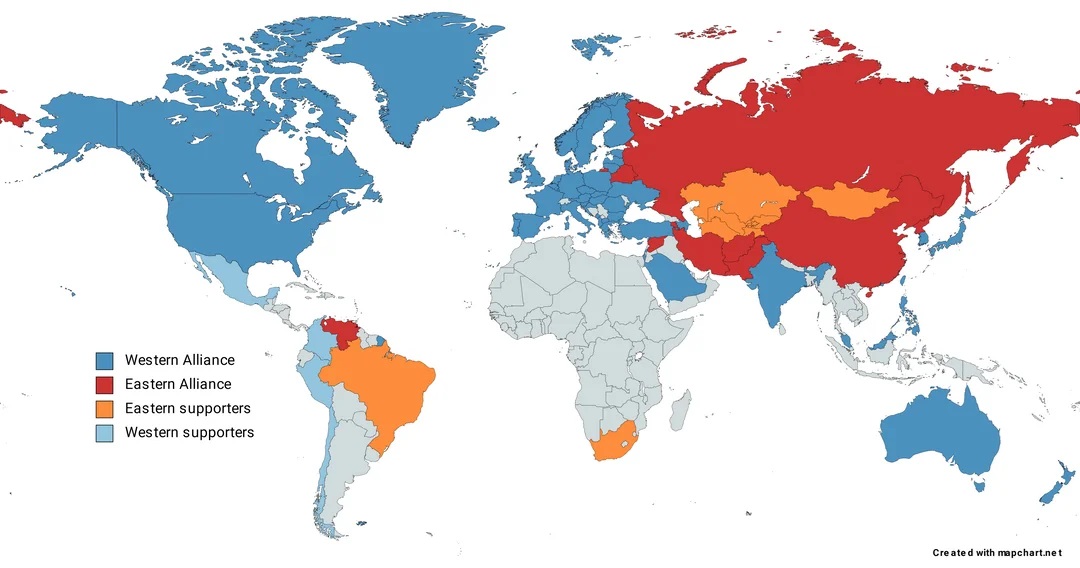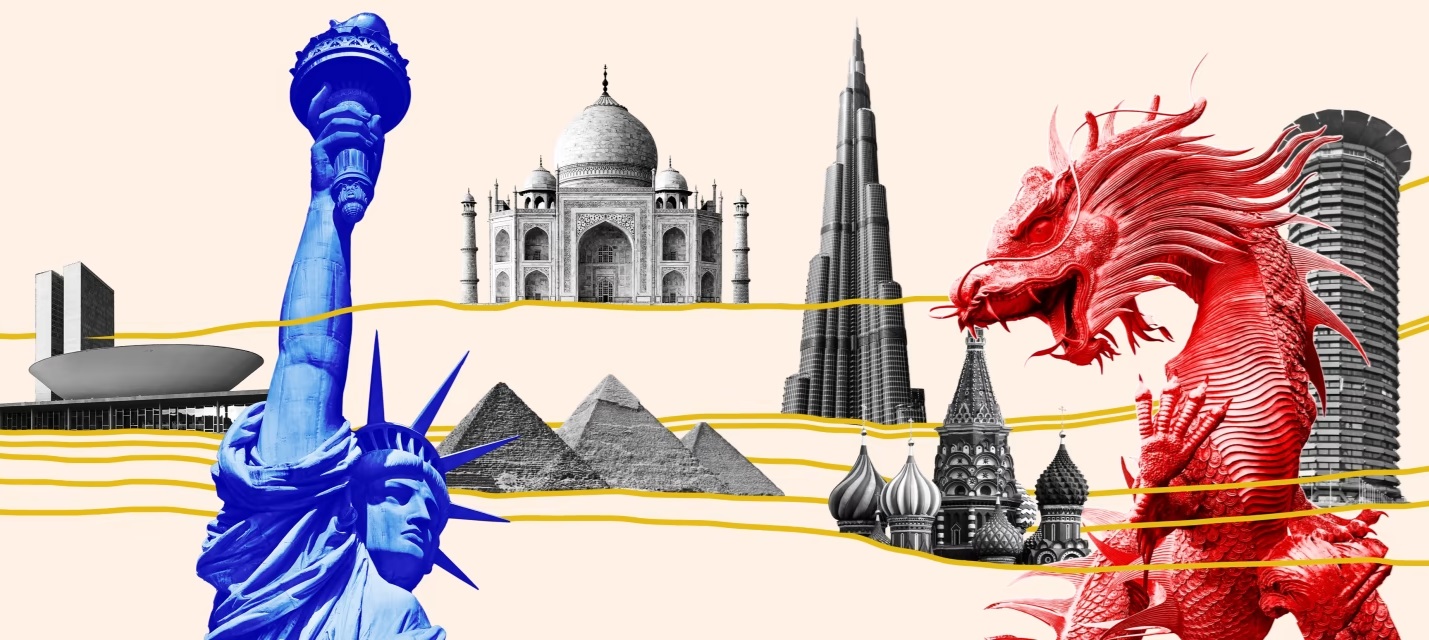अजब कहानी शहरों के विकास की
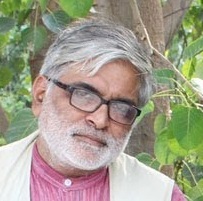 (अब ऐसा समय आ गया है जिसमें हमें विकास की अपनी समझ की गलती दिखाई देने लगी है, लेकिन फिर भी हम उसे मानना नहीं चाहते। यदि मान लेते तो शायद उसे बदलना नहीं, तो कम–से–कम सुधारना शुरु हो गया होता। ऐसे में कुछ आवाजें हमें बार–बार अपनी गलती का अहसास करवाती रहती हैं। प्रस्तुत है, इसी अहसास पर हिमालय में सक्रिय संस्था ‘हिमाल’ के अध्यक्ष रमेश मुमुक्षु का यह लेख।)
(अब ऐसा समय आ गया है जिसमें हमें विकास की अपनी समझ की गलती दिखाई देने लगी है, लेकिन फिर भी हम उसे मानना नहीं चाहते। यदि मान लेते तो शायद उसे बदलना नहीं, तो कम–से–कम सुधारना शुरु हो गया होता। ऐसे में कुछ आवाजें हमें बार–बार अपनी गलती का अहसास करवाती रहती हैं। प्रस्तुत है, इसी अहसास पर हिमालय में सक्रिय संस्था ‘हिमाल’ के अध्यक्ष रमेश मुमुक्षु का यह लेख।)
शुरुआत में शहर धीमे–धीमे, बे–आवाज बढ़ता है। खेत, खलिहान, जलस्रोत, जोहड़, तालाब, झील निगलता है, गाडियां सरपट दौड़ें, इसकी कोशिश करता है। एक बार शहर सुंदर हो गया तो उसको पर्यावरण की याद आने लगती है। अपने आस–पास सब ठीक रहे, जगत भले विनाश की ओर जाए। वो मैप देखता है और वहीं जाता है, जहां पर ‘सिक्स लेन’ और ‘फोर लेन’ की सड़क सरपट एसयूवी को ले जाये और किसी बड़े मोटल में रेस्ट करके आगे सरपट हो जाये। मेरे घर के पास नहीं, इसको दूसरे के घर ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए पुल, कारखाना। मेरे घर के बाजू में नहीं चाहिए, भले ही किसी और के घर के बाहर कुछ भी हो। जिसकी चलती है, वो रास्ते बदल देता है। एक फार्म हाउस के लिए सरकारी सड़क बदल जाती है। समग्रता से सोचना हम छोड़ चुके हैं, हम केवल अपने लिए ही सोचते हैं।
गंगोत्री के रास्ते में देवदार के हजारों पेड कटे, कोई अंतर नहीं, हमारी गाड़ी सरपट दौड़नी चाहिए। देवदार 100 साल में बढ़ता है। वह पिलखन नहीं है, जो दूसरे दशक में ही विशालकाय हो जाता है। मानेसर तक 21 किलोमीटर लंबे और छह मीटर चौड़े कांक्रीट और ऊंची मंजिलों से भरपूर ‘द्वारका एक्सप्रेस वे’ देखा तो मुझे लगा, ये जिन्न के दिए के जादू की तरह कहाँ से अवतरित हो गया। खेत–खलिहान और न जाने कितने जलस्रोत स्वाहा हो गए, इस विकास की यात्रा में, लेकिन ताज्जुब है, किसी की उफ तक नहीं आई। जिन्होंने वहां पर फ्लैट लिए वो कहते आ रहे हैं कि जल्दी ही कनेक्टिविटी हो जाएगी। सदियों से पुरखों द्वारा तैयार की गई खेती की उत्पादक जमीन कांक्रीट में तब्दील हो गई है। ये सब महानगर की त्रासदी है। ये विकास सच्चाई अथवा अनिवार्य है, यह कौन तय करेगा?
कौन द्वारका आना चाहता था, मेट्रो बनी तो डीलर की भाषा में कनेक्टिविटी से रेट बढ़ गए। अब कहते हैं, ‘द्वारका एक्सप्रेस वे’ की कनेक्टिविटी बनी तो फिर क्या है? पानी का एक बहुत विशाल और न ख़त्म होने वाला स्रोत नजफगढ़ झील है, लेकिन विकास और अदूरदर्शिता से वो भी संकट में है। विकास की बेतरतीव रफ्तार ने साहिबी/साबी नदी को रेवाड़ी के मसानी बैराज तक ही सीमित कर दिया है। अभी नजफगढ़ झील में सारा पानी विश्वप्रसिद्ध गुरुग्राम के सीवर से आकर इकट्ठा होता है। हालांकि अभी झील में रिचार्ज भी होने लगा है, लेकिन किसी को कुछ लेना–देना नहीं। विदेशी पक्षी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आते रहे हैं। ये प्राकृतिक अवसाद, नेचुरल डिप्रेशन है। ये खादर का इलाका है। वर्षा में जलभराव होता है और धीमे–धीमे वो चेनल के द्वारा यमुना नदी में जाता है, जिसको खोदकर गहरा और चौड़ा करके नजफगढ़ नाला बनता है। इसके अंदर वजीराबाद तक करीब 35 से ऊपर गंदे नाले गिरते हैं, जो यमुना नदी को दूषित करते हैं, लेकिन हम सब भूल गए हैं। हम को केवल ‘फोर बीएचके, पेंटहाउस, डुप्लेक्स जैसे शब्द ही याद रह गए हैं। पानी कहाँ से आयेगा, कोई परवाह नहीं। गुरुग्राम के लगभग सभी प्राकृतिक स्रोत खत्म हो चुके हैं। यमुना और गंगा के पानी पर निगाहें है, जबकि हिमालय के 285 विकासखंड पानी की कमी को झेल रहे हैं। जब प्राकृतिक स्रोत पर संकट आता है, तो नदी में पानी कैसे बढ सकेगा। लेकिन इतना कौन सोचे? अपना घर बचना चाहिए, दूसरे का जाता है, तो हमें क्या लेना–देना?
कब आएगी ये आवाज कि हमें नहीं चाहिए हिमालय में कोई और बड़ा बांध, नहीं चाहिए कोई बड़ी खदान, नहीं चाहिए बड़े कारखाने और हवाई–अड्डे, नहीं फोड़ना है, पर्वत के सीने को, नहीं घेरना है, सागर तट, नहीं चाहिए मुझे, उच्च हिमालय पर पर्यटन और नहीं चाहिए मुझे सारे संसाधन मेरे घर पर। विकास हो, लेकिन प्राकृतिक संवर्धन के साथ सतत विकास ही एक मात्र उद्देश्य हो। मेरा घर, मोहल्ला, शहर भी बचें और दूसरे की भी हम सोचें, ऐसा ‘माइंड सेट’ होना है। समग्रता से चिंतन करना है। द्वारका के विकास का असर कहाँ पर होगा? हम पानी किस नदी से लेंगे? उस नदी के उदगम से सागर तक जाने के क्या हाल हैं? नदी के किनारों पर कब्जे तो नहीं हैं, सागर के किनारों को हम घेर तो नहीं रहे। उच्च हिमालय को हम छेड़ तो नहीं रहे, जहां सीटी बजाने भर से ही पत्थर भरभरा के गिरने लगते हैं।
कहीं और विकास को देख हम खुश होते हैं, लेकिन मेरे घर के पास कुछ हुआ तो मैं दुःखी हो उठता हूँ। ये ‘होलिस्टिक’ सोच नहीं है। हम तो जड़, चेतन, सूक्ष्म, अति–सूक्ष्म की भी कामना करते हैं। समस्त पृथ्वी एवं ब्रह्मांड की चिंता और स्तुति करते हैं, तो हम संकुचित क्यों सोचे? नागरिक और सरकार को इस संकुचित सोच से उबरना होगा। किसी भी विकास परियोजना को जनता के सामने रखें और खुलकर चर्चा हो, तो विरोध की जरूरत ही नहीं होगी। विकास के साथ प्राकृतिक स्रोत का संरक्षण, संवर्धन पहली शर्त होनी चाहिए। कूड़े का निस्तारण कैसे होगा? दूषित जल का प्रबंध कैसे होगा? जल का अनुकूलतम एवं अधिकतम उपयोग कैसे होगा? ऐसी सोच के बिना समग्र एवं सतत, टिकाऊ विकास संभव ही नहीं है।
अभी ‘पर्यावरण इम्पैक्ट असेसमेंट-2020’ (ईआईए-2020) जैसा–का–तैसा लागू हुआ तो शिकायत भी नहीं हो सकेगी, ये भी हम सबको सोचना ही होगा। एक बात याद रखें कि कोई भी परियोजना ‘जनहित’ के नाम पर ही बनती है, जबकि जनता ने तो नहीं बोला और न ही उससे पूछा गया। इस पर हम सबको आगे आकर काम करना है। मुझे पुल नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिये, दूसरी ओर ले जाओ, मुझे बरसों ये सोच अधूरी जगी है। जहां ले जाओगे, उसके बारे में भी सोचो कि वहां पर क्या होगा? लेकिन मेरी बला से, कहीं भी जाए।
पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई भी प्रतिकार हो, उसका स्वागत तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारा दृष्टिकोण समग्र और सतत विकास की अवधारणा पर टिका हुआ होना चाहिए। सरकार, ठेकेदार और विकास के पुरोधा हमारी इसी संकुचित सोच का लाभ उठाते है। हमें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं। जब तक हम छोटा सोचेंगे, उतना ही हमको अनदेखा किया जाएगा। मेरे घर के पास नहीं, मेरे घर से दूर ले जाओ, क्योंकि आखिर ये मेरा ही है। मुझे अपना पेड़ बचाना है, भले दूसरों के जंगल साफ हो जाएं। मुझे सभी ओर सरपट दौड़ने वाली सड़क, पुल और ऊंचे पर्वतों पर रहने के लिए आरामगाह चाहिए। सरकार पहले सपना दिखाती है, सब सपने में मग्न हो जाते हैं। जब तक सपना किसी और के विनाश का होता है, तो कोई एतराज नहीं, लेकिन जब गाज अपने सिर पर गिरने लगती है तो बरबस सब कुछ याद आने लगता है। बस मैं ही बचूं, मेरा पेड़, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरी शांति, ये सब चलता है।
(सर्वोदय प्रेस सर्विस से साभार)