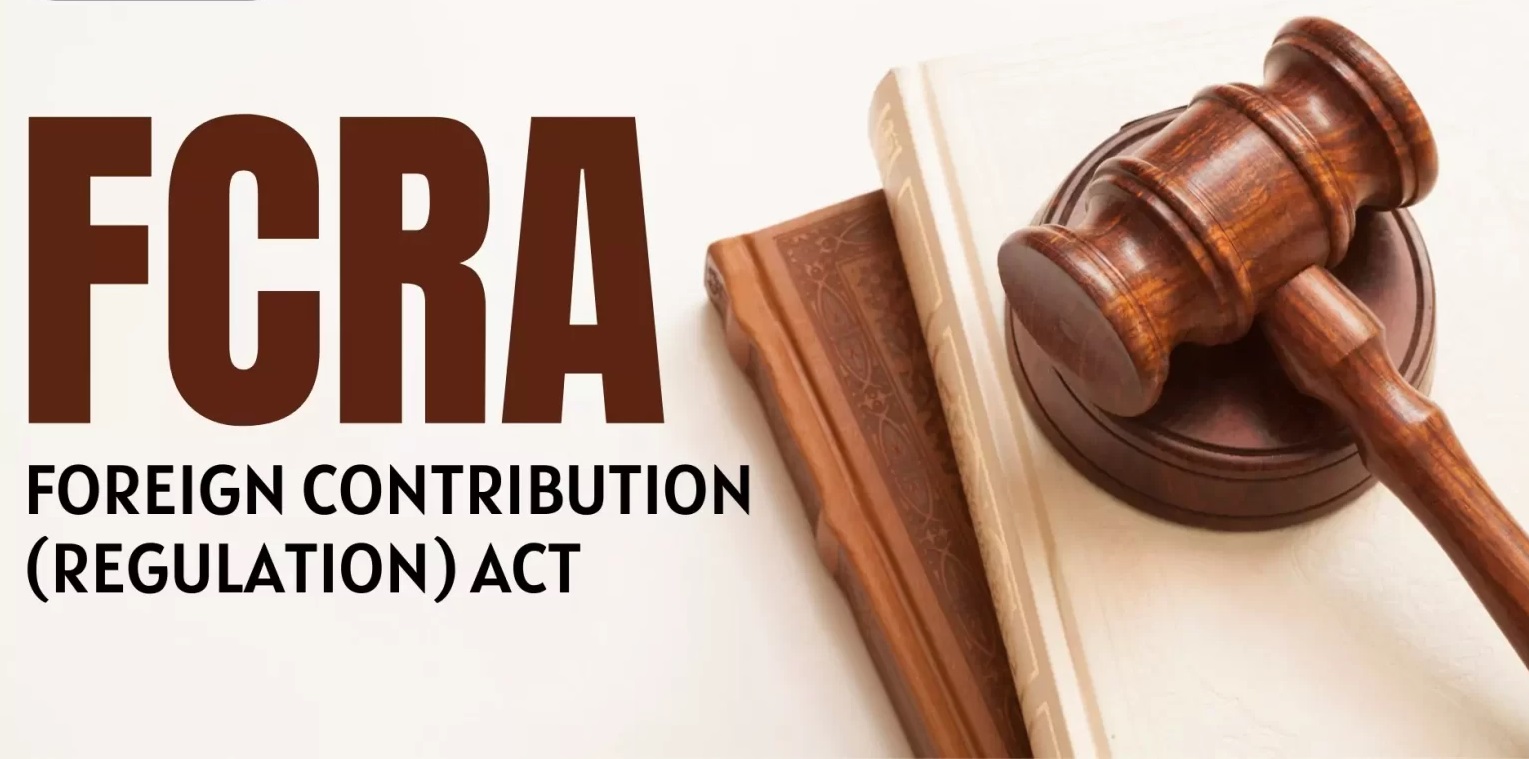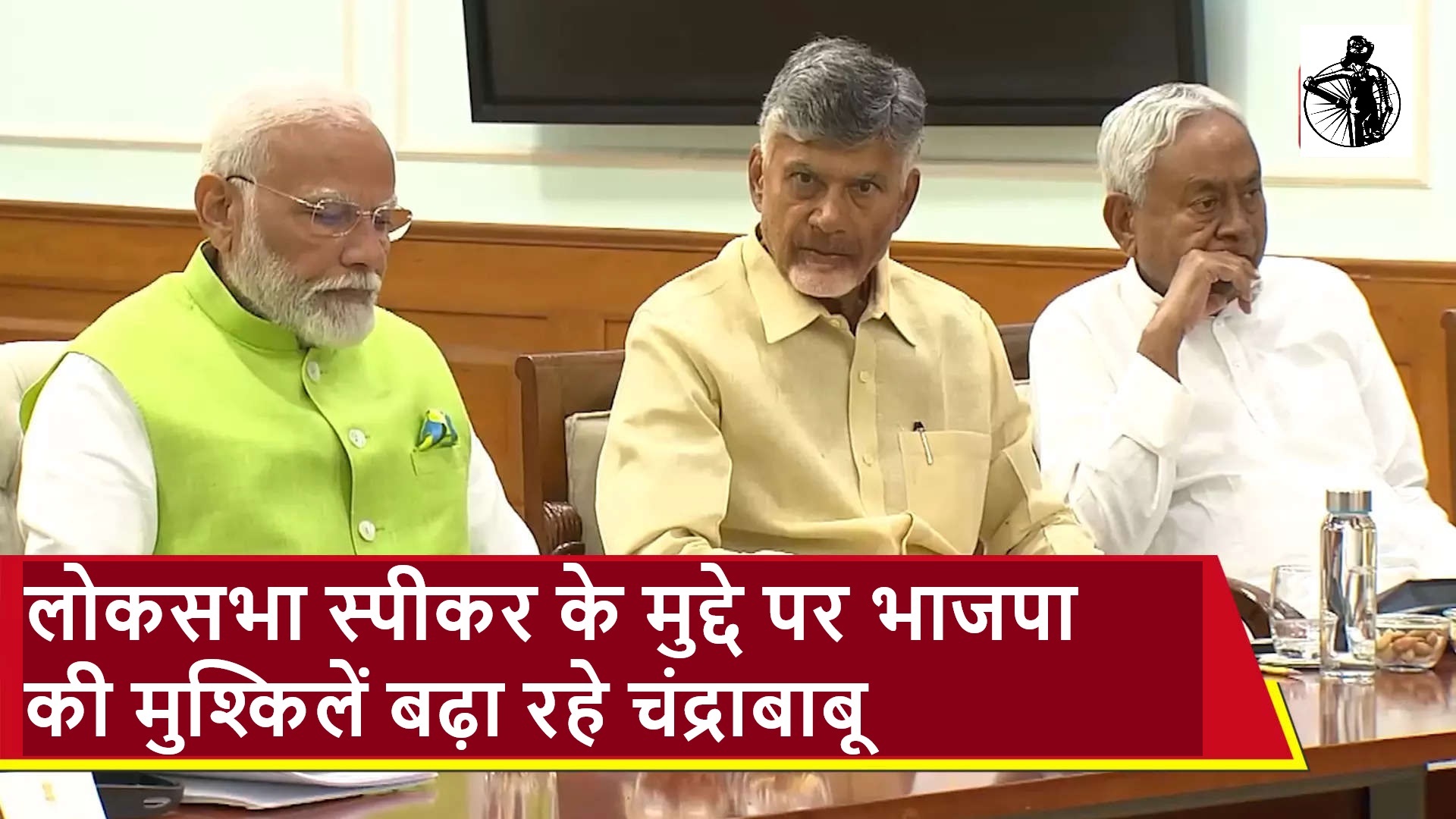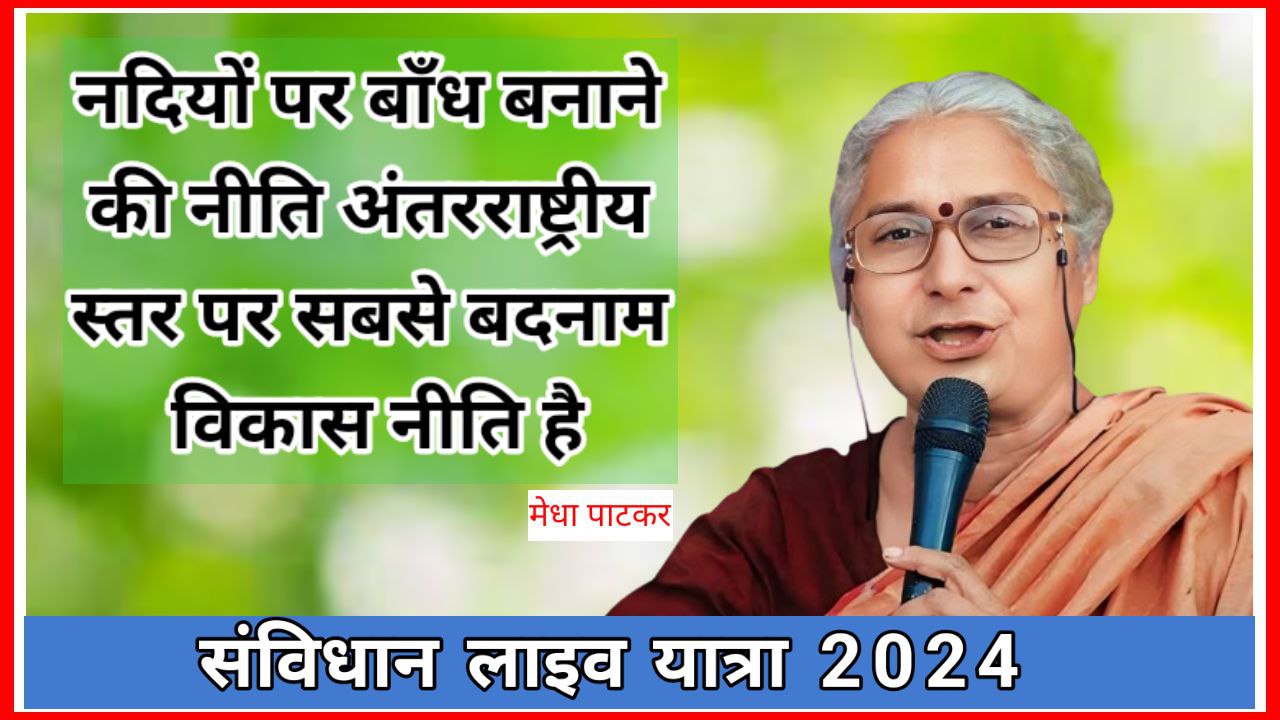कला और विचार का मेल
 बलराज साहनी। जेहन में नाम आते ही, काले पेंट और सफेद शर्ट में बोलते चेहरे वाला एक डॉक्टर याद आता है, या फिर ‘ए मेरे जोहराजबीं…’ गाता हुआ रौबीली मूंछों वाला कलाकार, या फिर अपने बाजुओं की ताकत की घोषणा करता मेहनतकश, या जमीन छिनने के दर्द के साथ रिक्शा खींचता शंभू महतो… या…. या…। ऐसे कितने ही ‘या’ हो सकते हैं, उस बेमिसाल कलाकार और संवेदनशील इंसान को याद करने के, जिसके लिए कला अभिव्यक्ति का साधन थी और अभिव्यक्ति थी, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की गरीब जनता की कराह। याद कीजिए कि बलराज साहनी के संबंध में ऊपर जितनी भी दृश्यनुमा घटनाओं का जिक्र किया गया है, उसमें एक कलाकार कहां खड़ा हुआ है? डॉक्टर गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहा है, प्रेम की अभिव्यक्ति का खूबसूरत गीत गाते हुए सौंदर्य की अमरता का बखान किया जा रहा है, कर्म को किस्मत से बड़ा बताते हुए मेहनत पर भरोसा किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की दौड़ में वैचारिक निस्तेजता के बीच बलराज साहनी का कद अपने समय के तमाम कलाकारों से बड़ा दिखाई देता है, तो इसकी वजह उनका वह जीवन है, जो फिल्मी चकाचौंध में कम दिखाई देता है।
बलराज साहनी। जेहन में नाम आते ही, काले पेंट और सफेद शर्ट में बोलते चेहरे वाला एक डॉक्टर याद आता है, या फिर ‘ए मेरे जोहराजबीं…’ गाता हुआ रौबीली मूंछों वाला कलाकार, या फिर अपने बाजुओं की ताकत की घोषणा करता मेहनतकश, या जमीन छिनने के दर्द के साथ रिक्शा खींचता शंभू महतो… या…. या…। ऐसे कितने ही ‘या’ हो सकते हैं, उस बेमिसाल कलाकार और संवेदनशील इंसान को याद करने के, जिसके लिए कला अभिव्यक्ति का साधन थी और अभिव्यक्ति थी, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की गरीब जनता की कराह। याद कीजिए कि बलराज साहनी के संबंध में ऊपर जितनी भी दृश्यनुमा घटनाओं का जिक्र किया गया है, उसमें एक कलाकार कहां खड़ा हुआ है? डॉक्टर गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहा है, प्रेम की अभिव्यक्ति का खूबसूरत गीत गाते हुए सौंदर्य की अमरता का बखान किया जा रहा है, कर्म को किस्मत से बड़ा बताते हुए मेहनत पर भरोसा किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की दौड़ में वैचारिक निस्तेजता के बीच बलराज साहनी का कद अपने समय के तमाम कलाकारों से बड़ा दिखाई देता है, तो इसकी वजह उनका वह जीवन है, जो फिल्मी चकाचौंध में कम दिखाई देता है।
1 मई 1913… रावलपिंडी! बलराज साहनी का जन्म और 1973 में उनकी आखिरी फिल्म आई, ‘गरम हवा’। इस फिल्म के आखिरी सीन में बलराज साहनी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जा रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल अंत में आशावादी नजरों से भारत में ही रहने का फैसला करते हैं। रावलपिंडी के गुलाम हिंदुस्तान और 1973 के उथल-पुथल भरे भारत के बीच बलराज साहनी का जीवन अपने कई रंगों में बिखरा पड़ा है। एक लेखक, अभिनेता, रंगकर्मी, रेडियोकर्मी, शिक्षक और बेहतरीन इंसान जैसे संबोधन बलराज साहनी की शख्सियत को पूरी तरह समझने के लिए नाकाफी हैं। लेकिन एक इकलौते सिरे से अगर इस बहुमुखी इंसान को समझना हो, तो वह है, उनका थियेटर से जुड़ाव। बलराज साहनी भारतीय जन नाट्य संघ से गहरे जुड़े थे। 1943 में मुंबई में इप्टा की स्थापना से लेकर आजीवन वे रंगकर्म के इस महत्वपूर्ण आंदोलन का हिस्सा रहे। उनके छोटे भाई भीष्म साहनी भी इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे। साम्यवादी विचारों का प्रभाव और जीवन जीने का सामूहिक तरीका बलराज साहनी के रंगकर्म और फिर उनकी सर्वश्रेष्ठ कलात्मक अभिव्यक्तियों में देखा जा सकता है। फिल्मी परदे पर बलराज जी ने जो पात्र अपने जादूई अभिनय से अमर बनाए है, यह अनायास नहीं है कि वे सभी इंसान की बराबरी, दुनिया की बेहतरी और मजलूम के हक की बात करते हैं। आज के दौर में जब पैसे के लिए कलाकार कोई भी रोल अभिनीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब समझना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे अपने पात्रों के चयन में बलराज जी इतने गंभीर और साफ थे। इस चयन की ऊर्जा उन्हें विचार से मिलती थी।
बलराज जी ने रावलपिंडी के बाद लाहौर का जीवन जिया। वहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद पिता के व्यवसाय में कुछ हाथ आजमाया। लेकिन यह उनकी उस अभिव्यक्ति को रास नहीं आ रहा था, जो दबी पड़ी थी, और जिसे बमार्फत थियेटर, फिल्म और लेखन बाहर आना था। उन्होंने शांति निकेतन का रुख किया। महात्मा गांधी के प्रभाव में भी आए, और फिर लंदन चले गए, बीबीसी में बतौर रेडियो अनाउंसर। वापस लौटे तो बलराज बदले-बदले थे। इस बीच उनकी कहानियां ‘हंस’ में छपने लगी थीं। लंदन से लौटने के बाद बलराज साहनी ने एक कहानी लिखी। चार साल की लेखन से दूरी, उस प्रतिभा पर भारी पड़ी, जो एक लेखक को जन्मजात मिलती है, लेकिन उसे अभ्यास से अर्जित और परिष्कृत किया जाता है। कहानी हंस में रिजेक्ट हो गई। यह चोट थी बलराज जी के लिए। उन्होंने कहानी लिखना बंद कर दिया। इससे पहले वह मुंबई इप्टा की फिल्म ‘धरती के लाल’ में अभिनय कर चुके थे। फिल्मों की छुट-पुट शुरुआत को मुकम्मल तार देने का वक्त आ चुका था और ‘काबुलीवाला’, ‘लाजवंती’, ‘हकीकत’, ‘दो बीघा जमीन’, ‘वक्त’, ‘दो रास्ते’ और ‘गरम हवा’ उनका इंतजार कर रही थीं। बलराज जी ने ऐसे कई यादगार रोल्स तो किए ही, उन्होंने पाकिस्तान और रूस की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सच्चाइयों की परतें भेदने वाले यात्रा वृतांतों को भी किताब की शक्ल दी।
‘बाजी’ की पटकथा और ‘गरम हवा’ के निर्देशन के दौरान बलराज जी की काम में डूबने की घटनाओं की लंबी श्रृंखला है, जिसे आज भी एके हंगल याद करते हुए मुस्कुरा उठते हैं। 13 अप्रैल 1973 को बलराज जी का निधन हो गया। इससे पहले गरम हवा बन चुकी थी। बलराज जी अब नहीं है, और हवा सिनेमा से लेकर थियेटर और साहित्य से लेकर समाज तक में गर्म है। क्या उनका अभिनय इस गर्म हवा में ठंडा और सकूनदेह है? साथ ही इंसान की कामयाबी और उसकी सच्चाई से भरापूरा? यकीनन हां।
(30 अप्रैल को जनवाणी में प्रकाशित)