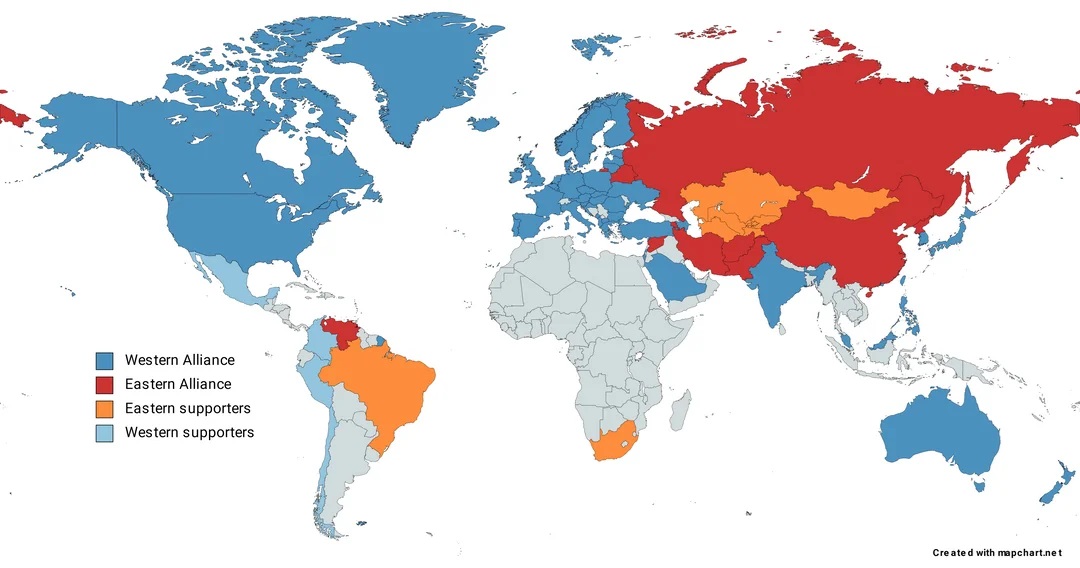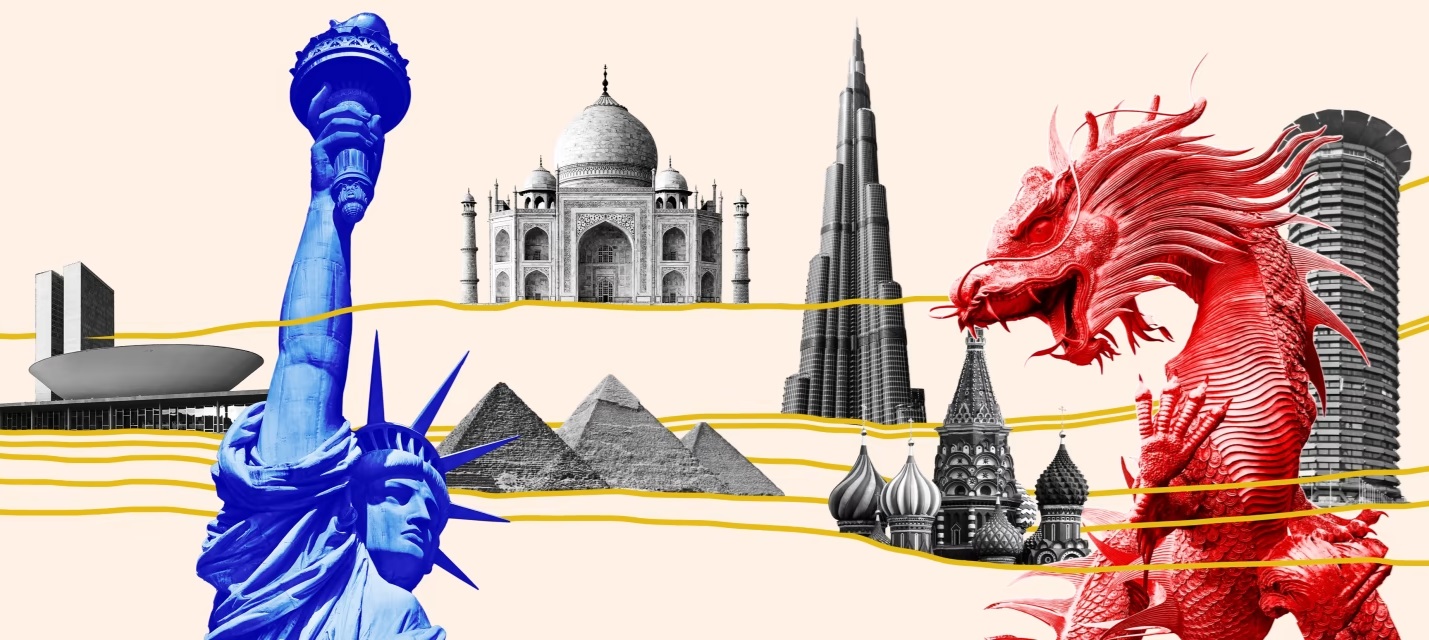NGO: सरकार की साथी, गैर-सरकारी संस्थाएं
वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली
 गैर-सरकारी समाजसेवी संस्थाएं (NGO) सरकार से समान दूरी रखते हुए उसे आइना दिखाते रहने के लिए भी खड़ी की जाती रही हैं, लेकिन आजकल इन संस्थाओं का चाल-चरित्र और चेहरा बदल-सा गया है। ‘एनजीओ’ (NGO) के नाम से पुकारी जाने वाली ये संस्थाएं अब सरकार से गलबहियां डालने को भी अपना काम समझने लगी हैं। ऐसे में क्या ये संस्थाएं (NGO) कारगर हो पाएंगी? प्रस्तुत है, इस विषय पर प्रकाश डालता सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण वैज्ञानिक वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली का यह लेख।
गैर-सरकारी समाजसेवी संस्थाएं (NGO) सरकार से समान दूरी रखते हुए उसे आइना दिखाते रहने के लिए भी खड़ी की जाती रही हैं, लेकिन आजकल इन संस्थाओं का चाल-चरित्र और चेहरा बदल-सा गया है। ‘एनजीओ’ (NGO) के नाम से पुकारी जाने वाली ये संस्थाएं अब सरकार से गलबहियां डालने को भी अपना काम समझने लगी हैं। ऐसे में क्या ये संस्थाएं (NGO) कारगर हो पाएंगी? प्रस्तुत है, इस विषय पर प्रकाश डालता सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण वैज्ञानिक वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली का यह लेख।
यह बहुत छुपी बात नहीं है कि आज अधिकांश पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं (NGO) के कर्णधार अपना व्यवहार ऐसा रखने में दक्ष होते जा रहे हैं जिससे वे जो दल तात्कालिक सत्ता में हो उनसे नजदीकियत के कारण मिलने वाले उपकारों व आभामण्डल के साये का लाभ उठा सकें। ऐसा व्यवहार उन संस्थाओं (NGO) का ही नहीं होता जो कमजोर होती हैं, बल्कि कार्पोरेट घरानों या उनके परिवार-जनों व्दारा प्रायोजित या संरक्षित संस्थाओं के सर्वेसर्वा भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे ढुलमुल आचरण अंगीकार करने वालों में सीधी रीढ़ की बेहद कमी दिखती है। सामाजिक संस्थाओं का नेताओं व सरकारों के नजदीक दिखने का मोह संस्थाओं की साख भी गिरा रहा है। सामाजिक संस्थायें (NGO) सामाजिक कार्यकर्ताओं व्दारा ही बनाई गईं या प्रायोजित हैं, इनमें काम करने वाले असामाजिक नहीं होंगे ऐसी गलतफहमी तो अब शायद ही कोई पालता हो।
जो संस्थायें अपने को सामाजिक कहती हों उनसे समाज के पक्ष में अपने को जोखिम में डालकर भी सच कहने की अपेक्षा तो की ही जानी चाहिए। फिर यदि वे अपने को गैर-सरकारी भी घोषित करती हों तो आशा यह भी रहती है कि वे सरकारी ‘गोद’ में बैठने या उनसे अपनी निकटता के प्रलोभन से बचें, किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। यही कारण है कि बालशोषण व बालश्रम के विरोध के स्वनाम-धन्य नायक उन सरकारों से पाये गये स्वागत से या उनके मंत्रियों से मिलने वाली गलबहियों से आल्हादित हो जाते हैं जिन सरकारों में बाल-शोषण रोकने पर ना के बराबर काम हो रहा है और जिनके यहां खुले आम होती बाल-मजदूरी को भी आंकड़ों में नहीं दिखाया जाता है।
नदियों का प्रदूषण रोकने के अभियानों के शुभारंभ या समापन का मंच उन सरकारी नेताओं को दे दिया जाता है, जो नदियों को चीर-भेदकर बांध और उनसे कमाने का लक्ष्य सर्वोपरी मानते हैं। हिमालय के घाव व हिमालय-वासियों की वेदना जिन सरकारों की कारगुजारी से बढ़ी हैं उन्ही को ‘हिमालय बचाओ’ जैसे सामाजिक अभियानों की भेंट तश्तरी में रखी मिल जाती है। अर्थात् जब अपना ही आयोजन हो, अपना ही मंच हो, अपना ही अवसर हो, तब भी आयोजक सामाजिक संस्थायें सरकारों को अपने आयोजनों में उनके कुशासन को दिखाने की हिम्मत नहीं करतीं।
कुल मिलाकर बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा की गोष्ठी हो या नदियों, गांवों, हिमालय-बचाओ की संगोष्ठी, उन्हीं सरकारों के मंत्री-मुख्यमंत्री या शीर्ष अधिकारी मुख्य-संबोधन करते दिखते हैं जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में ऐसे खतरों को बढ़ावा दिया है। ऐसी गैर-सरकारी सामाजिक संस्थायें अब अपवाद भी नहीं हैं जो कई बार राजनैतिक व कई बार स्वहित के कारणों से सरकारों का मुखौटा व भोंपू बनकर रह गई हैं। वे मुख्यमंत्री, मंत्रियों को समाज के उन सत्यों को देखने को मजबूर नहीं करतीं जिन्हें वे छवि खराब न होने के डर से एक सिरे से नकराते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि समाज में शोषण का प्रतिरोध व सही आंकड़ों को प्रस्तुत करने के साहस में कमी आती है।
सरकारों से लड़ना भी न पड़े व लोगों की नजर में आपकी गैर-सरकारी व सामाजिक होने की पहचान भी बनी रहे इसलिए कई पंजीकृत या अपंजीकृत गैर-सरकारी संस्थायें अपने को ‘डॅवलपमेंट एजेन्सी’ कहलाना पसन्द करती हैं। इनके एजेण्डा में सामाजिक आन्दोलनों में भागीदारी के लिए अपने या समाज को गतिशील व जागरूक करना नहीं होता। हालांकि ऐसी संस्थायें ‘परियोजना-मोड’ में वित्तीय-अनुबंधों में किये गये अपने कार्यों को भी सामाजिक कार्य ही मानती हैं। साथ ही सरकारों के साथ दिखना, बजाये उनके विरोध में जाने के, नीतिगत रूप से ज्यादा पसंद करती हैं। ऐसे में वे सरकारों के लिए चुनौतियां नहीं, बल्कि उनके लिए ‘चारा’ बन जाती हैं। अपनी ऐसी परिणतियों पर चिन्तित होते या ग्लानि अनुभव करने के बजाये वे इसे अपनी उपलब्धि मानती हैं कि उनकी संस्था के पदाधिकारी सत्तारूढ़ नेता, मंत्रियों, अधिकारियों के साथ मंच साझा करते हैं। दुखद यह रहता है कि साझा मंचों से गलत सरकारी आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण व बयानबाजी का तत्काल विरोध करने का साहस ऐसी ‘गोदी संस्थाओं’ के पदाधिकारी या प्रतिनिधि नहीं जुटा पाते। निस्संदेह ऐसा आचरण एक सामाजिक संस्था या सामाजिक कार्यकर्ता का नहीं हो सकता।
पांच दशकों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो मेरा अनुभव है कि ईमानदार, नि:स्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता व संस्थाओं की नियति सदैव प्रतिपक्ष के खेमे में ही दिखने की होती है। जब आप कुशासन या गलत नीतियों का प्रतिकार करने वाले या लोगों के दमन को रोकने के लिए खड़े होने वाले होंगे तो सत्तारूढ़ दल या प्रशासन आपके विरूध्द ही होगा, फिर भले ही सवाल स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा या मानव अधिकारों के हनन का हो। ऐसे में आप पर विपक्षियों के समर्थक होने का आरोप तो लगेगा ही। अब यदि विपक्ष, सत्तापक्ष बन जाता है और आप समाज के हित के लिए लड़ते हैं तो आप उसी पक्ष के विरोधी दिखेंगे जिसके समर्थक होने का लांछन आप पर पहले लगा था। बिना यह देखे कि पहले वे आपके अभियानों व मंतव्यों में साथ थे, आपको उनके जनविरोधी कार्यों का प्रतिकार सड़क या मंच पर करना ही होगा।
गैर-सरकारी संस्थायें अपने लिए ‘स्वतंत्र क्षेत्र’ के अंतर्गत संबोधन चाहती हैं तो भी उन्हें समाज के हित में सरकारों को आइना दिखाने का साहस बचाये व बनाये रखना चाहिए। परियोजनाओं में भी जनभागीदारी व लक्षित लाभार्थियों के लाभों को दिलाने में वे सरकारी परियोजनाओं को हाथ में ले सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं का तो और भी दायित्व है कि वे सरकारी परियोजनाओं के पैसों को जनता का ही योगदान मानें। ‘विश्वबैंक’ या अन्य वित्तीय संस्थाओं के कर्ज की वापसी जनता के पैसों से ही की जायेगी। वैसे भी सरकारी कर्मचारी का वेतन भत्ता भी जनता के पैसे से ही आता है।
(सप्रेस से साभार)